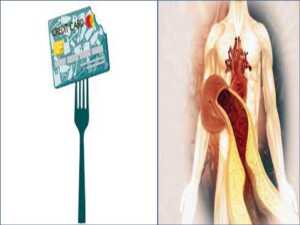ललित मौर्य
हम इंसान अपनी सांस के जरिए हर घंटे माइक्रोप्लास्टिक्स के करीब 16.2 कण निगल सकते हैं। निगले गए इस माइक्रोप्लास्टिक्स की यह मात्रा कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यदि हफ्ते भर निगले गए इन प्लास्टिक के महीन कणों को जमा किया जाए तो इनसे एक क्रेडिट कार्ड बनाने जितना प्लास्टिक इकट्ठा हो सकता है।

बता दें कि प्लास्टिक के अत्यंत महीन टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। इन कणों का आकार एक माइक्रोमीटर से पांच मिलीमीटर के बीच होता है। प्लास्टिक के इन महीन कणों में भी जहरीले प्रदूषक और केमिकल होते हैं जो स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ऐसे में सांस सम्बन्धी रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि सांस के जरिए प्लास्टिक के यह कण श्वसन तंत्र में कैसे यात्रा करते हैं। इसे समझने के लिए सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, उर्मिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी, कोमिला विश्वविद्यालय और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन किया है।

इस अध्ययन के नतीजे 13 जून 2023 को फिजिक्स ऑफ फ्लुइड्स नामक जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने श्वसन तंत्र के ऊपरी वायुमार्ग में माइक्रोप्लास्टिक्स के जमाव और परिवहन को समझने के लिए एक कम्प्यूटेशनल फ्लूड डायनामिक्स मॉडल विकसित किया है।
इस बारे में अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता मोहम्मद एस इस्लाम का कहना है कि, “माइक्रोप्लास्टिक के लाखों कण हवा, पानी और मिट्टी में पाए गए हैं। इतना ही नहीं वैश्विक स्तर पर इन कणों की मात्रा तेजी से बढ़ रहा है। नतीजनहवा में मौजूद इन कणों का घनत्व भी काफी बढ़ गया है।“

इंसान के प्लेसेंटा से लेकर रक्त में मिल चुके हैं माइक्रोप्लास्टिक के अंश
गौरतलब है कि 2022 में पहली बार इंसानी फेफड़ों में यह कण पाए गए थे। जो इस बात की चिंता को बढ़ाते हैं कि यह कण सांस सम्बन्धी बीमारियों के खतरों को किस तरह बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि अपने इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने श्वसन तंत्र में विभिन्न आकार और आकृतियों के कणों के प्रवाह का पता लगाया है।
यह कण आकार में 1.6 से 5.56 माइक्रोन जितने बड़े थे। वहीं इनकी आकृति गोलाकार, बेलनाकार और चतुष्फलकीय थी। माइक्रोप्लास्टिक्स के यह कण नाक, मुखग्रसनी और गले के पिछले हिस्सों में मुख्य तौर पर पाए गए थे, जो इनके हॉटस्पॉट भी थे।

गौरतलब है कि वैज्ञानिकों को अब तक इंसानों के रक्त और फेफड़ों के साथ नसों में भी माइक्रोप्लास्टिक के अंश मिल चुके हैं। वहीं जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अध्ययन में अजन्मे शिशुओं के प्लेसेंटा यानी गर्भनाल में भी माइक्रोप्लास्टिक के होने का पता चला था।
इंसानी शरीर में इनके मिलने के सबूत एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि वातावरण में बढ़ता प्लास्टिक का यह जहर न केवल हमारे वातावरण में बल्कि हमारी नसों और शरीर के अंगों तक में घुल चुका है।

इस प्रवाह के बारे में इस्लाम ने बताया कि, “हमारा वायुमार्ग बड़ा जटिल और आकार में असमान होता है। साथ ही नाक के छिद्र और मुखग्रसनी में हवा के प्रवाह का पैटर्न भी बहुत पेचीदा होता है। जो माइक्रोप्लास्टिक्स को प्रवाह के सामान्य पथ से दूर ले जाता है और इन विशिष्ट क्षेत्रों में जमा होने का कारण बनता है।“इसके साथ ही उनके मुताबिक प्रवाह की गति, कणों की जड़ता और विषम रचना भी जमाव को प्रभावित करती है।
रिसर्च के मुताबिक वायुमार्ग में प्लास्टिक के जमा होने की दर सांस लेने की स्थिति और माइक्रोप्लास्टिक के आकार जैसे कारकों से भी प्रभावित होती है। जब एयरफ्लो की दर अधिक होती है तो उसके चलते इन कणों का कम जमाव हुआ था। साथ ही माइक्रोप्लास्टिक्स के बड़े कण जिनका आकार करीब 5.56 माइक्रोन था वो छोटे कणों की तुलना में कहीं ज्यादा बार वायुमार्ग में जमा होना शुरू हो गए थे।

प्लास्टिक के यह महीन कण स्वास्थ्य को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बारे में जानकारी हालांकि इस अध्ययन में नहीं दी गई है। लेकिन जर्नल केमिकल रिसर्च टॉक्सिकोलॉजी में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक शरीर की कोशिकीय कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक बार जब प्लास्टिक के यह महीन कण सांस या किसी अन्य जरिए से शरीर में पहुंच जाते हैं तो वो कुछ दिनों में ही फेफड़ों की कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म और विकास को प्रभावित करके उन्हें धीमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं यह इन कोशिकाओं के आकार में भी बदलाव कर सकते हैं।
शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अध्ययन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां प्लास्टिक प्रदूषण या औद्योगिक गतिविधियों का स्तर काफी ऊंचा है, वहां सांस के जरिए माइक्रोप्लास्टिक्स के संपर्क में आने की चिंता को उजागर करता है। उन्हें उम्मीद है कि इसके नतीजे इससे बचाव और स्वास्थ्य जोखिम के मूल्याङ्कन में सुधार करने में मददगार साबित हो सकते हैं।
(‘न्यूज़ 18 हिंदी’ के साभार )