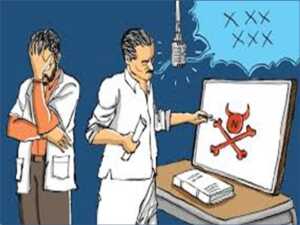वेदप्रिय
जब भी सामान्य व्यक्तियों के बीच विज्ञान या वैज्ञानिकता की बात चलती है तो एक सवाल अक्सर बीच में आकर खड़ा हो जाता है। सवाल प्रायः यही होता है कि एक वैज्ञानिक तो नास्तिक ही होता होगा। तो क्या विज्ञान की पढ़ाई नास्तिकता की पढ़ाई होती है? नहीं ,ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल यह सवाल ही विज्ञान से जुड़ा सवाल नहीं है। अधिकतर यह सवाल इसलिए भी किया जाता है कि कुछ व्यक्ति वैज्ञानिकता की बहस से या तो बचना चाहते हैं या इसे गलत दिशा देना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति शायद इसलिए ऐसा करते हों कि विज्ञान की यथोचित स्वीकार्यता स्वीकार करने पर उनके सामने जीवन -व्यवहार में परिवर्तन की दरकार न आ जाए। यह भी हो सकता है कि युगों से चली आ रही मान्यताएं जो अब झूठी पड़ती जा रही है और उन्हें त्यागने में उनका जी दुख पा रहा है ।

आस्तिकता व नास्तिकता का सवाल आस्था का सवाल है ।यह विज्ञान का सवाल नहीं है। एक वैज्ञानिक पर क्यों यह तोहमत लगाई जाए या अतिरिक्त दबाव डाला जाए कि वह इस सवाल का जवाब दे। एक वैज्ञानिक तो प्रकृति का अवलोकनकर्ता होता है। वह यह जानने- समझने की कोशिश करता है कि यह प्रकृति क्या है, यह कैसे व्यवहार करती है, यह ऐसी ही व्यवहार क्यों करती है, इसके विभिन्न घटकों के बीच क्या संबंध है, इस में घटित होने वाली घटनाओं की क्या प्रक्रिया है, आदि आदि।

आज तक कभी भी किसी बड़े वैज्ञानिक ने अपनी ऊर्जा या बौद्धिक श्रम इस प्रकार की बातों में नहीं लगाया कि वह नास्तिकता की खोज करें। कभी किसी बड़ी प्रयोगशाला में यह सब ढूंढने या जानने के लिए उपकरणों व प्रयोगों का सामान नहीं जुटाया गया और ना ही इस संबंध में कभी कोई प्रोजेक्ट तैयार किया गया कि वह नास्तिकता को सिद्ध करे। एक वैज्ञानिक हमेशा अपने मापन में आने वाले आंकड़ों व अवलोकनों पर भरोसा करता है।वह मापन में आने वाली भौतिक राशियों को अपनी खोज का आधार बनाता है। निस्संदेह वह कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है, लेकिन बेमतलब विचारों पर खोज करने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता।

यदि संयोगवश अनअपेक्षित पाया जाता है तो वह इस पर और ज्यादा प्रयोग करता है। और जब तक उसके पीछे के कारणों की पुष्टि नहीं हो जाती वह इसे स्वीकार नहीं करता। इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वह एक विधि की ओर बढ़ता है जिसे वह वैज्ञानिक विधि मानता है। यह निरंतर अपडेट होती रहती है। विवादास्पद परिस्थितियों में वैज्ञानिक, विज्ञान विधि पर ही सहमत होते हैं। लेकिन यह भी सही है कि हर युग में एक वैज्ञानिक को आस्तिकता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।

हम अपने विमर्शों में इंट्रडिसीप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं ।यदि इस दृष्टिकोण से आस्था के प्रश्नों को देखा जाए तो बहुत से अन्य कोणों के साथ हमें इसकी बात करनी पड़ेगी। यहां हम विज्ञान को छोड़ नहीं सकते। विज्ञान की मूल प्रवृत्ति ही है प्रश्न उठाना। विज्ञान, आस्था के सभी प्रस्तावित उत्तरों पर सवाल खड़े करना चाहेगा। यदि इन उत्तरों की व्याख्याएं स्पष्ट नहीं है या वस्तुनिष्ठ नहीं है तो विज्ञान इन्हें सहज स्वीकार नहीं करेगा। यदि काफी प्रयासों के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाए तो ‘चलो मान लेते हैं’ कि मनोस्थिति की एक बात है। यह क्षणिक लाचारी ही होनी चाहिए। लेकिन विज्ञान ने न जानने व ढूंढने की प्रवृत्ति से पीछे हटना नहीं स्वीकारा है। जानने की दिशा में वह आगे ही बढ़ता आया है। न मानने के लिए तर्क लगा अस्वीकृत करना होता है ।यह एक कठिन काम है। ‘चलो मान लेते हैं ‘ कहने में क्या जाता है। यह कहकर इतिश्री करना बड़ा आसान है। लेकिन इसके प्रभाव बहुत दूर तक जाते हैं। क्योंकि क्यों मान लिया गया है इस पर सवाल प्रायः नहीं उठाए जाते।

विश्वास करना (आस्था) क्या केवल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विषय है या इसका भी कोई जैव रासायनिक आधार है, या यह दोनों है। या इनके अलावा भी और कुछ है। हम सब जानते हैं कि हमारे विश्वासों से ही हमारा जीवन चलता है। यह सही है कि ये हमारे मस्तिष्क में बनते हैं। लेकिन ये कोई अकस्मात थोड़े ही बन गए। पहले ये हमारे प्रबोधन का हिस्सा बनते हैं। इनसे पहले पहले कुछ stimulii आते हैं। ये हर मनुष्य को एक सम्बल प्रदान करते हैं। विश्वासों के बनने के लिए ये stimulii ही काम करते हैं। ये कई स्रोतों से आते हैं। इनमें आंशिक व्यवहारिकता हो सकती है, इनमें परंपरामोह हो सकता है, न मानने के लिए किए जाने वाले बौद्धिक श्रम से बचते हुए सुगमता का रास्ता चुने जाने की प्रवृत्ति हो सकती है, संज्ञान प्रक्रिया की पेचीदगियों में कुछ छूटे हुए यथार्थ का अमूर्तिकरण भी इनमें शामिल हो सकता है। निस्संदेह परंपराएं एवं मान्यताएं हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और ये एक दिन में नहीं बनी हैं। इनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हो सकता है पूर्ण साक्ष्यों के अभाव में निभाए जाने की लाचारी हो या इनके पीछे सहजता में लेते हुए अधूरे सत्य को ही स्वीकार करने की मानसिकता काम कर रही हो। संस्कृति की बात विज्ञान में अभी नई-नई है। आज के दिन वैज्ञानिक अभी तो वैज्ञानिकता के मानक ही स्थापित कर रहे हैं। विज्ञान का अब तक का सफर तमाम प्रकार की अतार्किकताओं से लड़ते हुए तय हुआ है। यदि परंपराएं या मान्यताएं वर्तमान समाज के विकास में अवरोध बनती हैं तो हम इनका अनावश्यक बोझ क्यों ढोएं? हम इनकी पुनरसमीक्षा नई रोशनी में क्यों न करें? एक समय पर इनकी भूमिका किसी और रूप में रही होगी उस क्षेत्र की तात्कालिक जरूरत पर बहस कर सकते हैं।

(लेखक हरियाणा के वरिष्ठ विज्ञान लेखक एवं विज्ञान संचारक हैं तथा हरियाणा विज्ञान मंच से जुड़े हैं )