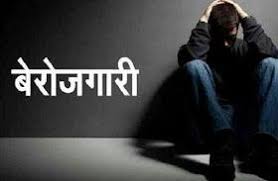डॉ. ईशान आनंद
कोरोना वायरस की महामारी से दुनिया भर में जान माल की काफी छति हुई है। भारत भी कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में कोरोना से आज तक साढ़े चार लाख से ज़्यादा लोगो की मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत में कोरोना के कारण हुई मौतों के संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना अधिक है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ है। 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले 7 प्रतिशत से छोटी हो गयी। अर्थव्यवस्था छोटी होने का मतलब देश में हो रहे उत्पादन में कमी आयी है। उत्पादन में कमी के कारण बेरोज़गारी आपने चरम पर पहुँच गयी।

समाज के भिन्न तबकों में बेरोज़गारी की समस्या अलग अलग स्तरों पर है। बढ़ती बेरोज़गारी का सबसे ज़्यादा असर भारत के युवाओं पर पड़ा है। युवाओं में बेरोज़गारी की दर लगभग 20 प्रतिशत है। यानी की हर पांच में से एक युवा रोज़गार ढूंढ़ने से सफल नहीं हो पा रहा है। बेरोज़गारी की समस्या ग्रेजुएट या उससे आगे की डिग्री प्राप्त करने वालों में भी बहुत बड़ी है। ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त लोगों में महिलाओं और सामाजिक तौर पर पिछड़े समुदायों में बेरोज़गारी दर औसत से काफी ज़्यादा है। यानी की बेरोज़गारी एक राष्ट्रीय समस्या तो है ही, साथ ही यह सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। 
पर क्या बेरोज़गारी सिर्फ कोरोना महामारी और उससे जुडी मंदी की देन है ? जी नहीं। ज़रूर कोरोना काल में बेरोज़गारी की समस्या बहुत बढ़ गयी है, पर इस समस्या की जड़ें काफी गहरी हैं। भारत सरकार के एक सर्वेक्षण ने पाया था की 2017-18 में बेरोज़गारी दर पिछले 45 वर्षों के सबसे अधिक स्तर पर थी।

बेरोज़गारी की इस समस्या के पीछे कुछ त्वरित कारण है और कुछ ढाँचागत। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2017 से चल रही आर्थिक तंगी एक त्वरित कारण है। इस तंगी के कई कारण हैं, पर इसमें नोटबंदी और जल्दबाज़ी में लागू की गयी जीएसटी की नीति प्रमुख है। इन नीतियों ने खासकर अनौपचारिक छेत्र की कमर तोड़ दी। अर्थव्यवस्था में मांग की कमी के कारण निजी पूँजी के निवेश में भरी कमी आई। समय पर इन समस्याओं का नीतिगत हल नहीं निकाला गया और 2017 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में बहुत कमी आयी, जिसके कारण बेरोज़गारी में बढ़ोतरी हुई।

ढाँचागत समस्या भारत के श्रम बाजार की बनावट से जुड़ी है। खेती से मामूली आमदनी, मशीनीकरण और बढ़ती आकांक्षाओं के कारण कृषि छेत्र आज के युवाओं को बेहतर रोज़गार नहीं दे पा रहा है। भारत में औद्योगीकरण का स्तर भी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। अच्छी नौकरियों की कमी के चलते बड़ी संख्या में कामगार स्वरोज़गार और अनौपचारिक रोज़गार में लगे हैं, जहाँ काम और आमदनी दोनों अस्थायी होती है।

बेरोज़गारी की इस समस्या का कोई शॉर्टकट समाधान नहीं है। ढांचागत बदलाव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। नरेगा को और मज़बूत करना और उसका शहरों में विस्तार एक सार्थक कदम हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ जैसे छेत्रों में भारी सरकारी निवेश से भी कई सारी बेहतर नौकरियां उपलब्ध होंगी। रोज़गार के लिए निजी पूँजी और बाजार पर निर्भर रहने की नीति विफल रही है। आज ज़रुरत है एक वैकल्पिक आर्थिक मॉडल की, जो रोज़गार को एक मौलिक अधिकार की तरह देखे और उसके लिए बाजारवाद से ऊपर उठ कर काम करे।
 ( डॉ. ईशान आनंद, ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में इकोनोमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )
( डॉ. ईशान आनंद, ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में इकोनोमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )